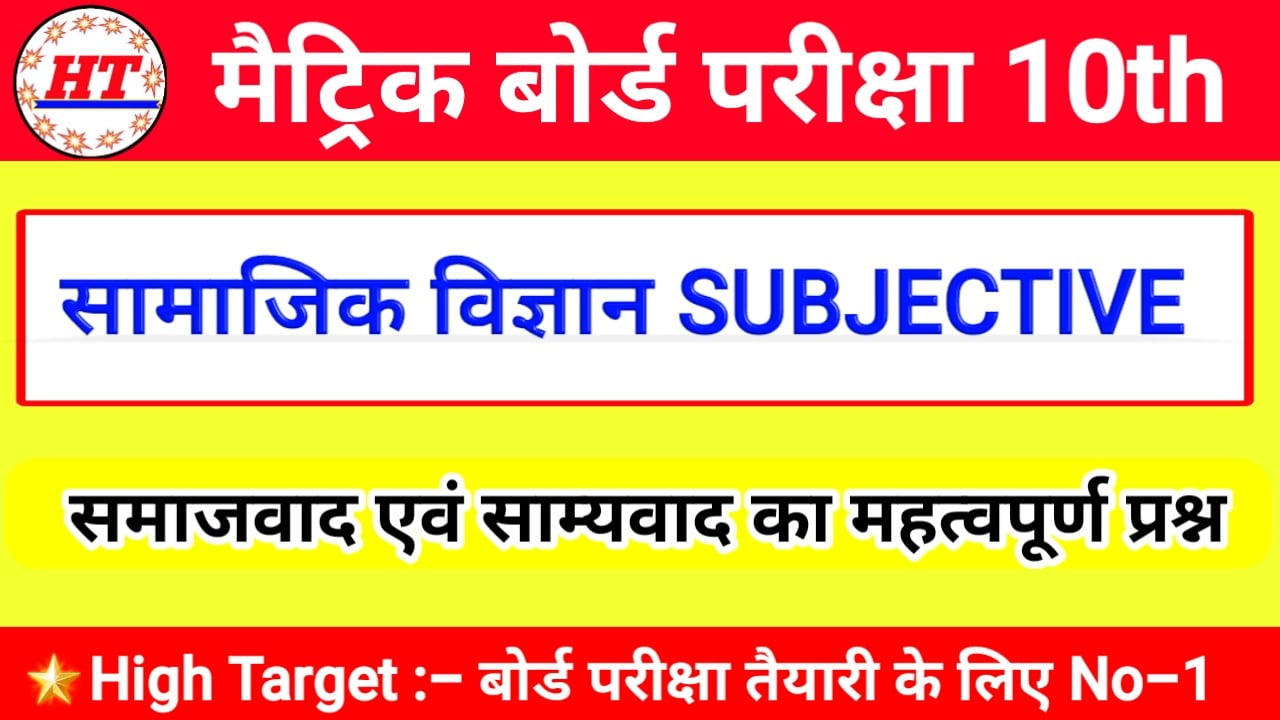
समाजवाद और साम्यवाद PART- 2 class 10 Subjective Long & Short Question Answer Matric Exam 2021
समाजवाद और साम्यवाद PART- 2 class 10
समाजवाद और साम्यवाद class 10|samajwad aur samyavad ka question paper|class 10th social science question answer in hindi|class 10th social science question paper 2021
1. रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें।
उत्तर- रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित थे –
(i) जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन : जॉर निकोलस द्वितीय कठोर एवं दमनात्मक नीति का संरक्षक था। वह राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था । उसे केवल अभिजात्य वर्ग और उच्च पदाधिकारियों का ही समर्थन प्राप्त था। इसकी पत्नी भी घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी। उस समय रासपुटीन की इच्छा ही कानून थी । वह नियुक्तियों, पदोन्नतियों तथा शासन के अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करता था । अतः गलत सलाहकार के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति दयनीत होती चली गई।
(ii) कृषकों की दयनीय स्थिति : यद्यपि 1861 में कृषि दासत्व को समाप्त कर दिया गया था, परन्तु किसानों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। रूस की कुल जनसंख्या का एक-तिहाई भाग भूमिहीन था जिन्हें जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था । इन कृषकों को कई तरह के करों का भुगतान करना पड़ता था। इनके पास पूँजी का अभाव था । ऐसी परिस्थिति में किसानों के पास क्रांति ही अंतिम विकल्प थी।
(iii) मजदूरों की दयनीय स्थिति : रूस के मजदूरों का काम एवं मजदूरी के आधार पर अधिकतम शोषण किया जाता था । मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार
नहीं थे। ये अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकते थे और न ही ‘मजदूर संघ’ बना सकते थे। रूसी मजदूर पूँजीवादी व्यवस्था तथा जारशाही की निरंकुशता
को समाप्त कर ‘सर्वहारा वर्ग’ का शासन स्थापित करना चाहते थे।
(iv) औद्योगिकीकरण की समस्या : रूस में राष्ट्रीय पूँजी का अभाव था अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूँजी पर निर्भरता बढ़ती गई। विदेशी पूँजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इस कारण लोगों में असंतोष व्याप्त था ।
(v) रूसीकरण की नीति : रूस में कई जातियाँ, कई धर्म तथा कई भाषाएँ प्रचलित थे। यहाँ स्लाव जाति सबसे महत्त्वपूर्ण थी। जार निकोलस द्वितीय ने रूसीकरण के लिए “एक जार एक धर्म” का नारा दिया तथा गैर-रूसी जनता का दमन किया । जार की इस नीति के खिलाफ गैर-रूसी जनता में असंतोष फैला और वे जारशाही के विरुद्ध हो गये।
(vi) जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति-1905 के रूस-जापान यद्ध में रूस की पराजय एशिया के एक छोटे देश से हो गई । इस पराजय के कारण रूस में 1905 में क्रांति हो गई। इस क्रांति ने अंततः 1917 में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
2. नई आर्थिक नीति क्या है ?
उत्तर – मार्च 1921 ई० में साम्यवादी दल के दसवें अधिवेशन में ‘नयी आर्थिक नीति’ की घोषणा लेनिन ने की। इस नीति के द्वारा लेनिन साम्यवादी सिद्धांत के साथ-ही-साथ पूँजीवादी विचारधारा को भी स्वीकार किया। इस नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों के आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना, नगरों और गाँवों के समस्त श्रमजीवी वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूत्रों को शासन के अधिकार में रखते हुए, आंशिक रूप से पूँजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था।
नई आर्थिक नीति के निम्नलिखित लाभ हुए –
(i) कृषि का पुनरुद्वार- कृषकों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बन्द कर दी गई एवं किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की गई ।
(iii) उद्योग – युद्ध सामग्री और उत्पादन के स्तर को ऊँचा करने के लिए आवश्यक था कि औद्योगिकीकरण तेजी से किया जाए । स्टालिन ने रूस को मशीन ‘ आयात करने वाले देश से मशीन निर्माण करने वाला देश बना दिया।
(iii) मुद्रा सुधार एवं व्यवस्था- गृहयुद्ध के कारण देश की मुद्रा का पूरी तरह अवमल्यन हो चुका था। अतः 1922 ई० में शासकीय बैंक को चवोनेत्स (10 स्वर्ण रूबल के बराबर) बैंक नोट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। 1924 में मुद्रा-सुधार करके रूबल की विनिमय दर स्थिर बना दी गयी।
(iv) छोटे उद्योग – सोवियत संघ में जहाँ बड़े उद्योगों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण था, वहीं कुछ छोटे उद्योगों का विराष्ट्रीयकरण किया गया। 1922 ई० में चार हजार छोटे उद्योगों को लाइसेंस.जारी किया गया ।
(v) श्रम और मजदुर सध जाति- जबरदस्ती श्रम करवाने और बराबर वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई । श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा भी दिया जाने लगा। कल मिलाकर नई आर्थिक नीति ने प्रथम महायद्ध और क्रांति के समय तथा गृहयुद्ध की अवधि में हुए विनाश से अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही सुधारने में बड़ी मदद की।
3. कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें ।
उत्तर – मार्क्स का जन्म 5 मई, 1818 ई० को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इसके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्क्स बोन विधि विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् 1936 में बर्लिन विधि विश्वविद्यालय चले आये। 1843 में अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। मार्क्स हींगेल के विचारों से प्रभावित थे । मार्क्स ने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मांण्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। 1844 ई० में मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंजेल्स से पेरिस में हुई । मार्क्स ने अपने मित्र फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ई० में “कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो’ (साम्यवादी घोषणा-पत्र) प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद कहा जाता है। इस घोषणा-पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। 1867 ई० में मार्क्स एवं एंजेल्स ने ‘दास-कैपिटल’ की रचना की जिसे ‘समाजवादियों की बाइबिल’ कहा जाता और यही दो पुस्तकें मार्क्सवादी दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत करती हैं जिसे 20वीं शताब्दी में साम्यवाद कहा गया है।
मार्क्स के सिद्धांत –
1. द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत
2. वर्ग-संघर्ष का सिद्धांत
3. इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या (इतिहास की आर्थिक व्याख्या)
4. मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत
5. वर्गहीन समाज की स्थापना की।
ऐतिहासिक भौतिकवाद- मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। मार्क्स ने इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन का मूल (जड़) आर्थिक शक्तियाँ हैं । उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ । इतिहास में पाँच चरण, अब तक दृष्टिगोचर हैं और छठा चरण आनेवाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स निम्नलिखित छह ऐतिहासिक चरण बताते हैं –
(1) आदिम साम्यवादी युग (Age of Primitive Communism)
(ii) दासता का युग (Slave Age)
(iii) सामन्ती युग (Feudal Age)
(iv) पूँजीवादी युग (Capitalist Age)
(v) समाजवादी युग (Socialist Age)
(vi) साम्यवादी युग (Communist Age)
मार्क्स के विचार में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यवर्गीय समाज का आधार नकद पूँजी है। यही मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है।
वर्गहीन समाज की स्थापना- मार्क्स का मानना था कि पूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग (मजदूर वर्ग) के बीच जो संघर्ष है उसमें निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग की विजय होगी और एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। मार्क्सवाद का आदर्श एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई अन्तर नहीं होता ।
4. यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें।
उत्तर – काल्पनिक (यटोपियन) समाजवादी समाजवादी विचारधारा की शुरुआत काल्पनिक समाजवादी विचारधारा के लोगों द्वारा शुरू की गई । सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के असली संस्थापक थे। इन्होंने ‘द न्यू क्रिश्चियनिटी’ (1825) में अपने समाजवादी विचारों का प्रतिपादन किया । साइमन का विचार था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से पुनर्गठन हो, श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाना चाहिए, प्रतियोगिता समाप्त होनी चाहिए, उत्पादन धनी वर्ग के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उसका सावधानी से नियंत्रण किया जाना चाहिए जिससे निर्धन श्रमिकों को लाभ हो सके। उसने घोषित किया, “प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पुरस्कार मिलना चाहिए।”
चार्ल्स फुरियेर ने असंख्य निर्धन श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सहकारी समुदायों को संगठित करने की योजना बनाई । इस प्रकार, सेंट साइमन और चार्ल्स फुरियेर दोनों यह मानते थे कि मजदूरों का कल्याण तभी सम्भव है जब पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा स्थापित नियंत्रण समाप्त हो जाए। परन्तु, इन दोनों की विचारधारा अव्यावहारिक सिद्ध हुई ।
1840 ई० के बाद लुई ब्लां फ्रांस का सबसे प्रभावशाली काल्पनिक समाजवादी विचारक और नेता था। उसने आर्थिक क्षेत्र में वैयक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का विरोध किया और राज्य से मजदूर के काम के अधिकार और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए ‘राष्ट्रीय कारखानों’ की माँग की । लुई ब्लाँ का विश्वास था कि क्रांतिकारी षड्यंत्र के जरिये सत्ता पर अधिकार कर समाजवाद लाया जा सकता है । लुई ब्लाँ का विश्वास था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। लुई ब्लाँ के सुधार कार्यक्रम अधिक व्यावहारिक थे।
फ्रांस से बाहर ब्रिटेन में रॉबर्ट ओवेन, विलियम थाम्पसन टॉमस हॉडस्किन, जान ग्रे जैसे काल्पनिक समाजवादी विचारक थे। इसने स्कॉटलैण्ड के न्यू लूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। उसने अपनी फैक्ट्री में अनेक सुधार कर अपने मजदूरों की हालत सुधारने का प्रयास किया। उसने मजदूरों के काम के घंटों में कमी की तथा उन्हें उचित वेतन दिया । मजदूरों के लिए साफ-सुथरे मकान बनवाये और आमोद-प्रमोद के केन्द्र स्थापित किये।
निष्कर्षतः, उपर्युक्त सभी काल्पनिक समाजवादी विचारक आरंभिक चिंतक थे। इन्होंने वर्ग-संघर्ष के बदले वर्ग-समन्वय पर बल दिया जो समाजवाद का आदर्शवादी टुष्टिकोण था। इन्होंने पूँजी और श्रम के बीच के संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। कार्ल मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा विश्व को दी। .
5. रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें।
उत्तर – रूसी क्रांति का प्रभाव-रूसी क्रांति के प्रभाव को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—
(क) सोवियत संघ
(ख) विश्व
(क) सोवियत संघ पर अक्टूबर क्रांति के निम्न प्रभाव पड़े –
(i) स्वेच्छाचारी शासन का अंत—जारशाही एवं कुलीनों के स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर दिया गया । तत्पश्चात् एक नवीन संविधान का निर्माण किया ‘गया। जिसके अनुसार वहाँ जनता के शासन की स्थापना हुई। –
(ii) सर्वहारा वर्ग का शासन— नए संविधान द्वारा मजदूरों को वोट देने का अधिकार मिला । देश की सम्पूर्ण संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की गई । उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का नियंत्रण हो गया। उत्पादन-व्यवस्था में निजी मुनाफे की भावना को निकाल दिया गया। .
(iii) साम्यवादी शासन की स्थापना-अक्टूबर क्रांति द्वारा सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। –
(iv) नवीन सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का विकास—सोवियत संघ में समाज में व्याप्त घोर असमानताएँ समाप्त हो गईं। समाज वर्गविहीन हो गया। अब समाज में एक ही वर्ग रहा और वह था—साम्यवादी नागरिक.। काम के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज एवं राज्य का कर्त्तव्य समझा गया।
(v) गैर-रूसी राष्ट्रों का विलयन-जिन गैर-रूसी राष्ट्रों पर जारशाही ने सत्ता स्थापित की थी वे सभी क्रांति के बाद गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ के अंग बन गए।
(vi) सभी जातियों को समानता का अधिकार— सोवियत संघ में सम्मिलित सभी जातियों की समानता को संविधान में कानूनी रूप दिया गया। उनकी भाषा तथा ‘संस्कृति का भी विकास हुआ ।
(ख) रूसी क्रांति का विश्व पर प्रभाव पड़ा- अक्टूबर क्रांति के विश्व पर पड़े प्रभाव को सकारात्मक एवं नकारात्मक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है।
सकारात्मक प्रभाव-
(i) 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी का सफलतापूर्वक सामना एवं द्वितीय विश्वयुद्ध से विश्व शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करने से विश्व के अन्य देशों—चीन, वियतनाम, युगोस्लाविया इत्यादि में साम्यवाद का प्रसार हुआ।
(ii) राज्यनियोजित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजना का विकास हुआ।
(iii) सोवियत संघ में किसानों एवं मजदूरों की सरकार स्थापित होने से सम्पूर्ण
विश्व में किसान एवं मजदूरों के महत्त्व में वृद्धि हुई।
नकारात्मक प्रभाव-
(i) सोवियत संघ एवं विश्व के कई देशों में साम्यवादी शासन स्थापित होने पर पूँजीवादी देशों (अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के देश) का तीव्र . विरोध हुआ । परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व पर 1990 तक (सोवियत
संघ के विघटन तक) शीतयुद्ध की काली छाया छाई रही।
(ii) सम्पूर्ण विश्व में पूँजीपतियों एवं मजदूरों के मध्य संघर्ष कटु होने लगा।
samajwad aur samyavad ka question paper
Geography ( भूगोल ) लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | भारत : संसाधन एवं उपयोग |
| 2 | कृषि ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 3 | निर्माण उद्योग ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 4 | परिवहन, संचार एवं व्यापार |
| 5 | बिहार : कृषि एवं वन संसाधन |
| 6 | मानचित्र अध्ययन ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
History ( इतिहास ) लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | यूरोप में राष्ट्रवाद |
| 2 | समाजवाद एवं साम्यवाद |
| 3 | हिंद-चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन |
| 4 | भारत में राष्ट्रवाद |
| 5 | अर्थव्यवस्था और आजीविका |
| 6 | शहरीकरण एवं शहरी जीवन |
| 7 | व्यापार और भूमंडलीकरण |
| 8 | प्रेस-संस्कृति एवं राष्ट्रवाद |
Political Science लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी |
| 2 | सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली |
| 3 | लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष |
| 4 | लोकतंत्र की उपलब्धियाँ |
| 5 | लोकतंत्र की चुनौतियाँ |
Economics ( अर्थशास्त्र ) लघु उत्तरीय प्रश्न
| 1 | अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास |
| 2 | राज्य एवं राष्ट्र की आय |
| 3 | मुद्रा, बचत एवं साख |
| 4 | हमारी वित्तीय संस्थाएँ |
| 5 | रोजगार एवं सेवाएँ |
| 6 | वैश्वीकरण ( लघु उत्तरीय प्रश्न ) |
| 7 | उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण |
Aapda Prabandhan Subjective 2022
| 1 | प्राकृतिक आपदा : एक परिचय |



